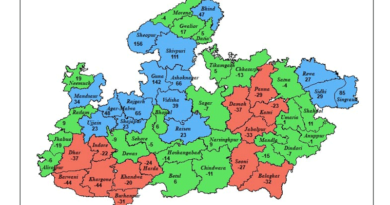भारी पड़ेगी भूजल की अनदेखी
25 जनवरी 2021 भोपाल ।जब से हमारे देश में कुंओं, बावडिय़ों का प्रचलन हुआ है तभी से भूजल के महत्व को समझा जाने लगा है। ‘पर्शियन व्हील’ (रेहट) के आगमन से भूजल का प्रयोग आसान हो गया और सिंचाई के लिए भी भूजल का प्रयोग होने लगा। फिर हैंडपंप और ट्यूबवेल का जमाना आ गया। नतीजे में भूजल दोहन में भारी तेजी आ गई। सरकारी ट्यूबवेल के अलावा निजी ट्यूबवेल भी लगने लगे। अनियंत्रित दोहन के चलते भूजल स्तर में गिरावट भी आने लगी।
भूजल एक सामुदायिक संसाधन है, किन्तु निजी ट्यूबवेल प्रचलन से इस संसाधन का अनायास ही निजीकरण होता गया। निजी ट्यूबवेल कृषि और उद्योगों के लिए लगाए गए, वहीं पेयजल आपूर्ति के लिए हैंडपंप का प्रचलन बढ़ता गया। भूजल स्तर में अति दोहन के कारण आई गिरावट को रोकने और नियंत्रित दोहन के लिए कानूनी प्रावधान भी किये जाने लगे। सन् 2005 में नया ‘भूजल प्रबन्धन अधिनियम’ और 2006 में नियम बनाए गए। इसके अनुसार भूजल प्रबन्धन को व्यवस्थित करने के प्रयास हो रहे हैं। ‘सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड’ के अनुसार देश के चंडीगढ़, पंजाब, पुदुचेरी, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, दादरा-नगर हवेली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल और मेघालय में 2016-17 के मुकाबले भूजल के ज्यादा दोहन से भूजल स्तर कम होता जा रहा है।
वर्ष 2017-18 में भूजल में औसत 9 मीटर की गिरावट आ गई थी। देश में 253 ब्लॉक अति दोहन के कारण ‘नाजुक स्थिति’ में, 681 ब्लॉक ‘अर्ध-नाजुक स्थिति’ में और 4520 ब्लॉक ‘सुरक्षित स्थिति’ में हैं। अति दोहन ग्रस्त ब्लॉकों की संख्या में हिमाचल प्रदेश भी कर्नाटक, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब आदि राज्यों की श्रेणी में आ गया है।
हिमाचल प्रदेश में 2005 में ‘भूजल अधिनियम’ और 2006 में उसके नियम बनाए जाने के बाद ‘भूजल प्राधिकरण’ का गठन हुआ। प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि वह यह ध्यान रखे कि भूजल का दोहन प्राकृतिक तौर पर भूजल पुनर्भरण की क्षमता से ज्यादा न हो और इस तरह पैदा असंतुलन का प्रबन्धन और नियन्त्रण किया जा सके। भूजल का डाटा बनाया जाए और उसका लगातार नवीकरण किया जाए। भूजल दोहन के लिए परमिट देना, भूजल प्रयोग करने वालों की सूची रखना, रिग मालिकों की सूची रखना, भूजल पुनर्भरण स्थलों की पहचान और वर्षा जल-संग्रहण से भूजल भरण को बढ़ाने के प्रयास करना भी प्राधिकरण की ही जिम्मेदारी है।
हिमाचल प्रदेश में 1990 में हैंड पंप लगाने का क्रम शुरू हुआ था जिसके लिए तकनीकी सहयोग देने के लिए भूगर्भ शास्त्री की दैनिक वेतन भोगी के आधार पर नियुक्ति की गई थी। धीरे-धीरे हैंडपंप और ट्यूबवेल कार्यक्रम लोगों में काफी लोकप्रिय हो गया। इसलिए इसमें राजनैतिक हस्तक्षेप बढ़ता गया। उस दौर में हमारे क्षेत्र में भी हैंडपंप के लिए सर्वेक्षण हुआ। मैंने भी अपने गांव में भी हैंडपंप लगाने की प्रार्थना की तो मुझे समझाया गया कि यहाँ भूजल उपलब्ध नहीं हो सकता। यहां भूगर्भीय चट्टानों और मिट्टी की संरचना ऐसी है जिसमें भूजल संचय की क्षमता नहीं है। यदि पंप लग भी जाए तो उसमें पानी नहीं आएगा। शुरू में यदि आ भी गया तो सतही पानी होगा जो दस बीस दिन में सूख जाएगा। बाद में दो-तीन वर्षों में कुछ लोगों ने दो-तीन जगहों पर हैण्डपंप लगवाए जो राजनैतिक निर्णय से लग भी गए, किन्तु पानी नहीं दे पाए। यह खेल सारे प्रदेश में हुआ और अभी भी चल ही रहा है।
इसके पीछे कई तरह के स्वार्थ भी जुड़ गए हैं। अभी फि़लहाल हैंडपंप लगाने पर प्रतिबन्ध लग गया है, किन्तु ट्यूबवेल तो लग ही रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अब तक 40,000 हैंडपंप और 8000 से अधिक ट्यूबवेल सरकारी क्षेत्र में लगाए जा चुके हैं और निजी क्षेत्र में कितने लगे हैं उसकी कोई जानकारी नहीं है। यदि सफल हैंडपंपों का सर्वे किया जाए तो बहुत से सूखे पड़े हैंडपंप दिख जाएंगे। बहुत से पंप ऐसे स्थलों पर भी लगाए गए हैं जहां सतही जल उपलब्ध है। उससे कूह्ले निकाल कर पुरानी कुह्लों की व्यवस्था को सुधार कर बिना भूजल को छेड़े सिंचाई हेतु जल आपूर्ति की जा सकती है या नल द्वारा पेयजल दिया जा सकता है। औद्योगिक क्षेत्रों में भी उद्योगों की जरूरतों की आपूर्ती हेतु भूजल का भारी दोहन हो रहा है। इसके अलावा कई उद्योगों द्वारा उद्योगों का गंदा, प्रदूषित पानी भूजल में डाल दिया जाता है। इससे दोहरा नुकसान होता है। एक तो भूजल स्तर नीचे गिर रहा है दूसरे, जो बचा हुआ भूजल है वह प्रदूषित हो जाता है। इस लापरवाही का ही परिणाम है कि आज हिमाचल के कई क्षेत्र भूजल दोहन के मामले में ‘अर्ध नाजुक’ स्तर पर पंहुच गए हैं।
ऊना जिले में पिछले 10 वर्षों में भूजल दो मीटर नीचे चला गया है। सोलन के नालागढ़ क्षेत्र में 6 मीटर नीचे चला गया है। काला अम्ब और काँगड़ा, हमीरपुर क्षेत्र भी खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। यानि एक ओर तो भूजल के स्तर में गिरावट का खतरा है और दूसरी ओर सतही जल के सूखते जाने का संकट खड़ा हो रहा है। आखिर सतही जलस्रोत भी भूजल से ही निकलते हैं और अत्यधिक दोहन के कारण बहुत से जलस्रोत सूख गए हैं। छोटे नदी नालों का पानी भी कई जगह सूखकर कम हो रहा है। इसलिए भूजल को गंभीरता से लेना होगा। ‘भूजल प्राधिकरण’ को भी ज्यादा सक्रियता दिखानी होगी। इसमें हाइड्रोलॉजी विज्ञानं के जानकारों की भूमिका मुख्य होनी चाहिए।
भूजल दोहन के सभी फैसले वैज्ञानिक आधार पर लिए जाने चाहिए, वोट की राजनीति के आधार पर नहीं। भूजल पुनर्भरण के प्रयासों को गति देनी होगी। वर्षा जल संग्रहण और रिचार्जिंग वेल उन क्षेत्रों में जरूरी होने चाहिए जहां भूजल स्तर में गिरावट दर्ज की जा रही है। अनावश्यक रूप से हर कहीं ट्यूबवेल की स्वीकृति देना भी ठीक नहीं है। उन्हीं स्थलों पर उनकी स्वीकृति दी जाए जहां भूजल स्तर में दोहन और पुनर्भरण में संतुलन साधना संभव है। भूजल स्तर का डाटा सर्वेक्षण एक सतत् प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे पता रहे कि कहां क्या सावधानी बरतने की जरूरत है।
महत्वपूर्ण खबर : महाविद्यालय द्वारा विश्व मृदा दिवस का आयोजन