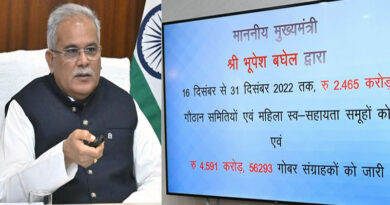संतरे की उन्नत खेती
- दुर्गाशंकर मीणा, तकनीकी सहायक,
- डॉ. मूलाराम, सहायक आचार्य, जयराज सिंह गौड़
- मुकुट बिहारी, कृषि पर्यवेक्षक
कृषि अनुसंधान केंद्र, मण्डोर (कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)
Email:-dstameena1997@gmail.com
2 फरवरी 2022, संतरे की उन्नत खेती – भारत में केले के पश्चात नींबू प्रजाति के फलों का तीसरा स्थान है इसमें सर्दी तथा गर्मी सहन करने की क्षमता होने के कारण नींबू प्रजाति का कोई ना कोई फल लगभग सभी प्रांतों में उगाया जाता है। इन नींबू वर्गीय फलों में संतरा भी एक महत्वपूर्ण फल है। संतरे को वानस्पतिक रूप से सिट्रस रिटीकुलेटा के नाम से जाना जाता है। भारत में नींबू प्रजाति के फलों में संतरे का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है इसे मेंडेरीन भी कहते हैं। संतरा अपनी सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसके साथ-साथ इसमें विटामिन ’ए’ और ’बी’ भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। देश के अंदर संतरे का कुल क्षेत्रफल 4.28 लाख हेक्टेयर है जिससे 51.01 लाख टन उत्पादन होता हैं।
भूमि
संतरे की खेती लगभग सभी प्रकार की अच्छे जल निकास वाली जीवांश युक्त भूमि में की जा सकती है, परंतु गहरी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। भूमि की गहराई 2 मीटर हो। मृदा का पीएच 4.5 से 7.5 उचित रहता है। इसकी सफलतम खेती के लिए अवमृदा कंकरीली पथरीली व कठोर नहीं होनी चाहिए।
उन्नत किस्में
भारत में उगाई जाने वाली किस्मों में नागपुरी संतरा, खासी संतरा, कुर्ग संतरा, पंजाब देसी, दार्जिलिंग संतरा व लाहौर लोकल आदि प्रमुख हैं। भारतीय संतरा में नागपुर संतरा सर्वोपरि हैं एवं विश्व के सर्वोत्तम संतरा में इसका स्थान प्रमुख हैं। किंग तथा विलोलीफ के संकरण से तैयार किन्नों की किस्म पंजाब और राजस्थान में व्यवसायिक महत्व की किस्म है।
प्रवर्धन
संतरे का वानस्पतिक प्रवर्धन कलिकायन विधि द्वारा किया जाता है। कलिकायन के लिये मूलवृन्त के रूप में जट्टी खट्टी, जम्भिरी, रंगपुर लाइम, किलओप्टरा मेन्डेरिन, ट्रायर सिट्रेन्ज तथा करना खट्टा काम में लेते हैं। मूलवृन्त फरवरी माह मे तैयार किये जाते है। लगभग एक वर्ष आयु का मूलवृन्त कलिकायन के लिये उपयुक्त रहता है। साधारणत: शील्ड एवं पैच कलिकायन फरवरी से मार्च व सितम्बर – अक्टूबर में किया जाये।
पौधा रोपण
कलिकायन किये गये पौधे दूसरे वर्ष जब लगभग 60 सेमी. के हो जाये तो पौधारोपण हेतु उपयुक्त माने जाते हैं। संतरे के पौधे लगाने के लिए 90 घन सेमी. आकार के गढ्ढे मई-जून में 6×6 मीटर की दूरी पर खोदे जाते हैं। उत्तरी भारत में पौधे लगाने का उचित समय जुलाई-अगस्त है। पौधा लगाने से पूर्व प्रत्येक गढ्ढे को 20 किलोग्राम गोबर की खाद, 1 किलोग्राम सुपर फास्फेट व मिट्टी के मिश्रण से भरें। दीमक के नियंत्रण के लिए मिथाइल पेराथियान 50-100 ग्राम प्रति गढ्ढा दें।
गोबर की खाद, सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा दिसम्बर-जनवरी में दें। यूरिया की 1/3 मात्रा फरवरी में फूल आने के पहले तथा शेष 1/3 मात्रा अप्रेल में फल बनने के बाद और शेष मात्रा अगस्त माह के अन्तिम सप्ताह में देवें। संतरा में फरवरी व जुलाई माह में गौण तत्वों का छिडक़ाव करना उचित रहता है। इसके लिये 550 ग्राम जिंक सल्फेट, 300 ग्राम कॉपर सल्फेट, 250 ग्राम मैंगनीज सल्फेट, 200 ग्राम मैग्नेशियम सल्फेट, 100 ग्राम बोरिक एसिड, 200 ग्राम फेरस सल्फेट व 900 ग्राम चूना लेकर 100 लीटर पानी में घोल बनाकर छिडक़ाव करें।
सिंचाई
सर्दी में दो सप्ताह व गर्मी में एक सप्ताह के अंतराल पर सिंचाई करें। फल लगते समय पानी की कमी से फल झडऩे लगते हैं। फल पकने के समय पानी की कमी से फल सिकुड़ जाते है व रस की प्रतिशत मात्रा घट जाती है। अत: जब सन्तरे का उद्यान फलन में हो तब आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। खाद देने के बाद सिंचाई करना परम आवश्यक है। कटाई-छंटाई संतरे का सुन्दर ढांचा बनाने के लिए प्रारम्भिक वर्षो मे कटाई-छंटाई की जाती है। फल देने वाले पौधो को कटाई-छंटाई की कम आवश्यकता होती है, परन्तु सूखी व रोगग्रस्त टहनियों को काटते रहें।
उपज एवं भण्डारण
कलिकायन द्वारा तैयार किये गये पौधे 3-5 वर्ष की आयु में फल देते हैं। प्राय: पुष्पन के 8 से 9 माह बाद फल पक कर तैयार हो जाते है। संतरे के फलों का रंग हल्का पीला हो जाये तब इन्हें तोड़ लेें। 600 से 800 फल तथा औसतन 70 से 80 किग्रा. प्रति पौधा प्राप्त होती है। संतरा के फलों को 5-6 डिग्री सेल्सियस तापक्रम व 85-90 प्रतिशत आपेक्षिक आद्र्रता पर 4 महीने तक भण्डारित किया जा सकता है।
फलों का गिरना
सामान्यत: माल्टा में तुड़ाई के लगभग पांच सप्ताह पहले से फल गिरने लगते हैं, इसकी रोकथाम हेतु 2, 4-डी (10 पीपीएम) या एनएए150 पीपीएम) का छिडक़ाव करें। इसके अतिरिक्त फलन के समय भूमि में समुचित नमी बनाये रखें।
यदि फलन के समय किसी कवक जनित रोग का प्रकोप हो तो उसके नियंत्रण का उचित उपाय करना लाभकारी रहता है।
कीट
नींबू की तितली- तितली की लटें पत्तियों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। इससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है। इसके नियंत्रण के लिये लटों को पौधों से पकड़ कर मिट्टी के तेल में डालें। क्विनालफास 25 ई.सी. का 1.5 मिली./लीटर पानी में घोल बनाकर छिडक़ाव करना चाहिए।
फल चूसक – कीट फलों से रस चूस कर नुकसान करता है। प्रभावित फल पीला पडक़र सूख जाता है और गुणवत्ता भी कम हो जाती है। इस कीट के नियंत्रण के लिये मैलाथियॉन 50 ई.सी. 1 मिली./लीटर पानी का घोल का छिडक़ाव करें। कीट को आकर्षित करने के लिये प्रलोभक का भी उपयोग करना चाहिए। प्रलोभक में 100 ग्राम शक्कर के 1 लीटर घोल में 10 मिली. मेलाथियॉन मिलाया जाता है।
लीफ माइनर – यह कीट वर्षा ऋतु में नुकसान पहुंचाता है। यह पत्तियों की निचली सतह को क्षतिग्रस्त कर पत्तियों में सुरंग बनाता है। इस कीट के नियंत्रण हेतु मिथाइल डिमेटॉन 25 ई.सी. या क्विनालफास 25 ई.सी. का 1.5 मिली./लीटर पानी में घोल बनाकर छिडक़ें।
मूलग्रन्थी (सूत्रकृमि) – यह नींबू प्रजाति के फलों की जड़ों को नुकसान पहुँचाता है। इसके प्रकोप से फल छोटे व कम लगते हंै। नुकसान पहुंचाता है जिससे पत्तियाँ पीली पड़ कर टहनियाँ सूखने लगती इसके नियंत्रण के लिये कार्बोफ्यूरॉन 3 जी. 20 ग्राम/पौधा देना चाहिए।
व्याधियाँ
नींबू का केंकर – यह रोग जेन्थोमोनास सिट्राई नामक जीवाणु द्वारा होता है। रोग से प्रभावित पत्तियों, फलों व टहनियों पर भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते है। फलों पर पीले, खुरदरे धब्बे बन जाने से गुणवत्ता प्रभावित होती है। कागजी नींबू इससे ज्यादा प्रभावित होते है। केंकर की रोकथाम के लिये 20 ग्राम एग्रोमाइसीन अथवा 8 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिडक़ाव करना चाहिए। नये रोग रहित पौधों का चुनाव करें तथा पौधों पर रोपण से पूर्व 4:4:50 बोर्डो मिश्रण छिडक़ें।
गमोसिस – यह तना सडऩ रोग है जिसमें तने से भूमि के पास व टहनियों के ग्रसित भाग से गोंद जैसा पदार्थ निकलता है। इस गोंद से छाल प्रभावित होकर नष्ट हो जाती है। रोग के अधिक प्रकोप से पौधा नष्ट हो जाता है। रोग के नियंत्रण के लिये छाल से गोंद हटाकर ब्लाईटॉक्स-50 0.3 प्रतिशत का छिडक़ाव करना चाहिए। इस दवा का छिडक़ाव पौधों पर भी किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त बाग का उचित प्रबंधन भी रोग से बचाव करता है।
सूखा रोग (डाई बैक) – इस रोग में टहनियाँ ऊपर से नीचे की तरफ सूख कर भूरी हो जाती है। पत्तियों पर भूरे बेंगनी धब्बे बनने से सूख कर गिर जाती है। इससे उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पौधा नष्ट हो जाता है। नियंत्रण के लिये रोगी भाग को काट कर अलग करें एवं मेन्कोजेब 2 ग्राम/लीटर पानी का घोल का छिडक़ाव करें। इसके अतिरिक्त फरवरी व अप्रैल माह में सूक्ष्म तत्वों का पौधों पर छिडक़ें।
महत्वपूर्ण खबर: बीज उत्पादक ही बीज गुणवत्ता के जिम्मेदार हों